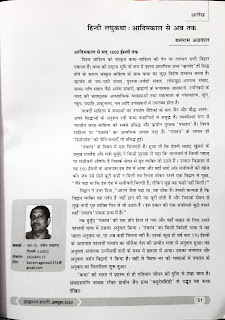प्रस्तुत है, अपेक्षाकृत लम्बे उक्त लेख की पहली कड़ी :
आदिम काल से सन् 1800 ई. तक
विश्व साहित्य को संस्कृत कथा-साहित्य की देन पर लगभग सभी विद्वान एकमत हैं। कथा की उद्गम भूमि के रूप में पहला प्रामाणिक ग्रंथ ‘ऋग्वेद’ ही सिद्ध होने के कारण संस्कृत साहित्य के साथ कथा का कुछ विशेष सम्बन्ध बनता है। ऋग्वेद के यम-यमी संवाद, पुरुरवा-उर्वशी संवाद, लोपामुद्रा-अगस्त्य संवाद, सरमा-पणि संवाद जैसे अनेक संवादों, ब्राह्मणों के रूपात्मक आख्यानों, उपनिषदों के नारद की भावमूलक आध्यात्मिक व्याख्याओं तथा महाभारत के गंगावतरण, शृंग, नहुष, ययाति, शकुन्तला, नल आदि जैसे उपाख्यानों में उपलब्ध होता है।
परवर्ती साहित्य में कथाओं का उपयोग वैदिकों के बाद जैन व बौद्ध आदि धार्मिक संप्रदायों ने अपने-अपने सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए किया। जैन और बौद्ध संप्रदाय अपने-अपने सिद्धांतों के अनुरूप रची कथा-कहानियों से समृद्ध हैं। व्यवस्थित रूप से भारतीय कथा-साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुस्तक ‘पंचतंत्र’ है। विश्व साहित्य पर ‘पंचतंत्र’ का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। ‘पंचतंत्र’ के समान ही ‘हितोपदेश’ की नीति कथाएँ भी प्रसिद्ध हुईं।
‘पंचतंत्र’ के बारे में एक किंवदंति खासी प्रसिद्ध है। हुआ यों कि, ईरानी सम्राट् खुसरो के प्रमुख राजवैद्य और मंत्री बुर्जुए ने किसी पुस्तक में पढ़ा कि भारतवर्ष में किसी पहाड़ पर संजीवनी औषधि है जिसके सेवन से मृत व्यक्ति जी उठते हैं । उत्कट जिज्ञासा से वह 550 ई. के आसपास इस देश में आया और यहाँ चारों ओर संजीवनी की खोज की । जब उसे ऐसी बूटी कहीं न मिली तब निराश होकर उसने एक विद्वान् से पूछा, “मैंने पढ़ा था कि इस देश में संजीवनी मिलती है; लेकिन मुझे वह कहीं नहीं मिली?”
विद्वान ने उत्तर दिया, “आपने जैसा पढ़ा था, वह ठीक है। हमारी मान्यता है कि विद्वान् व्यक्ति वह पर्वत है जहाँ ज्ञान की यह बूटी होती है और जिसके सेवन से मूर्ख-रूपी मृत व्यक्ति फिर से जी उठता है । इस प्रकार की एक संजीवनी बूटी हमारे यहाँ पंचतंत्र नामक ग्रन्थ में है।”
तब बुर्जुए पंचतंत्र की एक प्रति ईरान ले गया और वहाँ सम्राट के लिए उसने पहलवी भाषा में उसका अनुवाद किया । पंचतंत्र का किसी विदेशी भाषा में वह पहला अनुवाद था, पर अब कहीं मिलता नहीं है। उसके कुछ ही वर्ष बाद 570 ई. के आसपास पहलवी पंचतंत्र का सीरिया देश की प्राचीन भाषा में अनुवाद हुआ। वह अनुवाद अचानक उन्नीसवीं शती के मध्य भाग में प्रकाश में आया। उसका सम्पादन और अनुवाद जर्मन विद्वानों ने किया है। वहीं से विश्वभर की भाषाओं में पंचतंत्र के अनुवाद का सिलसिला शुरू हुआ।
‘कथा’ को भारत में प्रारम्भ से ही गतिमान जीवन की दृष्टि से देखा जाता है। संघदासगणि वाचक रचित प्राचीन जैन ग्रन्थ ‘वसुदेवहिंडी’ से उद्धृत यह कथा देखिए—
चलते चलते वसुदेव को थका हुआ जान, अंशुमान ने कहा, ”आर्यपुत्र! क्या मैं आपको ले चलूँ? यदि नहीं, तो आप मुझे ले चलिए।“
वसुदेव ने सोचा—थकान के कारण पैर लड़खड़ा रहे हैं, ऐसी हालत में यह मुझे कैसे लेकर चल सकता है? यह राजपुत्र सुकुमार है। मैं ही इसे क्यों न ले चलूँ? यह सोच उसने कहा, “आओ मित्र! चढ़ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ।”
अंशुमान ने हँसकर उत्तर दिया, “आर्यपुत्र! इस तरह किसी को मार्ग में लेकर नहीं चला जाता। यदि कोई थकान के कारण थके-माँदे व्यक्ति को रोचक कथाएँ सुनाता चले, तो इसे ‘ले-चलना’ कहते हैं। इससे थकान दूर हो जाती है।”
वसुदेव ने कहा, “ऐसी बात है तो कोई रोचक कथा सुनाओ। तुम्हीं इस कला में कुशल हो।”
सन् 1801 ई॰ से 1870 ई॰ तक
सन् 1800 ई॰ तक का लगभग समूचा कथा साहित्य पद्यमय है। लिखित साहित्य के गद्यमय होने का जैसे चलन ही नहीं था। समकालीन हिन्दी लघुकथा क्योंकि खड़ीबोली गद्य साहित्य की कथा विधा है, इसलिए सन् 1800 ई॰ तक के समूचे समय को ‘लघुकथा का वैदिक युग’ माना जा सकता है।
‘खड़ीबोली’ शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1803 ई. में लल्लूलाल ने ‘प्रेमसागर’ के संबंध में सूचना देते हुए किया।
कलकत्ते से छपा हिन्दी का पहला (साप्ताहिक) पत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’ (30 मई 1826 ई.) एक ऐतिहासिक घटना रही। उसके पीछे हिन्दी गद्य-निर्माण की विराट संभावनाएँ छिपी थीं। हिन्दी लघुकथा का सफ़र भी ‘उदंत मार्तण्ड’ के प्रकाशन से ही शुरू हो गया था। ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ के ‘आधुनिक गद्य:संवत् 1900 से 1925 तक’ (अर्थात् सन् 1843 ई से 1868 ई तक) खण्ड में शुक्ल जी ने ‘उदंत मार्तण्ड’ को ‘संवाद पत्र’ बताते हुए लिखा है—‘यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया।’ इसमें 'खड़ी बोली' का 'मध्यदेशीय भाषा' के नाम से उल्लेख किया गया है।’ लघुकथा की दृष्टि से उससे उल्लेखनीय उद्धरण यह है जिसे हमने ‘यशी वकील’ शीर्षक दिया है।
एक यशी वकील वकालत का काम करते-करते बुड्ढा होकर अपने दामाद को यह काम सौंप के आप सुचित हुआ। दामाद कई दिन काम करके एक दिन आया ओ प्रसन्न होकर बोला, ‘हे महाराज! आपने जो फलाने का पुराना वो संगीन मोकद्दमा हमें सौंपा था, सो आज फैसला हुआ।’
यह सुनकर वकील पछता करके बोला, ‘तुमने सत्यानाश किया। उस मोकद्दमे से हमारे बाप बड़े थे, तिस पीछे हमारे बाप मरती समय हमें हाथ उठाकर के दे गए ओ हमने भी उसको बना रखा ओ अब तक भलीभाँति अपना दिन कटा ओ वही मोकद्दमा तुमको सौंप कर समझा था कि तुम भी अपने बेटे-पोते-परोतों तक पलोगे; पर तुम थोड़े से दिनों में उसे खो बैठे।’
1857 की क्रान्ति के बाद भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्नीसवीं शताब्दी में गद्य-निर्माण की चेष्टाएँ कितनी तेज और पुष्ट थीं, इसका प्रमाण ‘कविवचन सुधा’ (1867 ई.), ‘हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ (1873 ई.), ‘बिहार बंधु’(1874 ई. / कहीं-कहीं इसका काल 1872 ई. भी लिखा है, लेकिन उस काल की फाइलें अप्राप्य हैं), ‘भारत मित्र’ (1878 ई.), ‘सार सुधानिधि’ (1879 ई.) और ‘उचितवक्ता (1880 ई.) के पन्नों पर लिखी इबारत है। इस काल के रचनाकारों, पत्रकारों, विचारकों, वक्ताओं ने कई-कई दायित्वों का निर्वाह एक-साथ किया। उन्होंने गद्य की भाषा को तो सँवारा ही, स्वाधीनता आंदोलन में भी स्वयं को बनाये रखा। जिस तरह 1857 ई. में स्वाधीनता-सेनानियों ने ‘रोटी और कमल’ को परस्पर संकेत का ‘कोड’ बनाया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वाधीनता की आग को सुलगाने और सुलगाए रखने का कार्य संकेत-प्रधान साहित्य रचकर किया। इस दिशा में उनकी रचना ‘अंधेर नगरी चौपट्ट राजा’ तो सब परिचित हैं ही, ‘मर्सिया’ और ‘परिहासिनी’ से कम लोग परिचित हैं। ‘मर्सिया’ से रुष्ट होकर सरकार ने उनके पत्रों की खरीद पर रोक लगा दी थी। तब उन्होंने ‘हास्य’ द्वारा संकेत का मार्ग अपनाया। ‘परिहासिनी’ में उनके द्वारा रचित हास-परिहास और चुटकिले आदि संग्रहीत हैं। अनेक चुटकिलों के माध्यम से ही भारतेंदु ने जन-जागरण का दायित्व निर्वाह किया। वे अच्छी तरह जानते थे कि ब्रिटिश शासन से जुड़े छोटे-बड़े सभी अधिकारी लिखे और बोले जा रहे शब्दों पर ‘गिद्धों और कुत्तों’ जैसी चेष्टाएँ रखते हैं। गिद्ध की आँखें तेज होती हैं और कुत्ते के कान। अत: 1870 ई. से गद्यपरक लघुकथा का आधुनिक काल विधिवत् शुरू हुआ जिसका श्रीगणेश निश्चित रूप से भारतेंदु ने किया।
सन् 1871 ई॰ से 1900 ई॰ तक
‘उदंत मार्तंड’ का प्रकाशन बंद होने के लगभग 41 वर्ष बाद भारतेंदु हरिश्चन्द्र द्वारा ‘कविवचन सुधा’ (5 अगस्त 1867 ई॰) के प्रकाशन काल तक भी, मौलिक पद्य लेखन के प्रमाण तो खूब मिलते हैं, गद्य लेखन के नाम पर कुछ पुराने ग्रंथों का अनुवाद ही अधिक प्राप्त होता है, मौलिक गद्य-लेखन प्राय: नहीं मिलता। सन् 1874 में ‘बिहार बंधु’ में छपी कुछ लघु आकारीय कथापरक रचनाओं का जिक्र डॉ॰ रामनिरंजन परिमलेंदु ने किया है। डॉ॰ परिमलेंदु के अनुसार—‘बिहार बन्धु’ के अति आरम्भिक अंकों में ‘नीति’ स्तम्भ के अन्तर्गत अनेक लघु कथाएँ प्रकाशित हुई थीं।
भारतेंदु ने अंग्रेज शासकों और भारतीय रईसों, जमींदारों आदि को केंद्र में रखकर अपने समय के लगभग सभी पत्रों में ‘चोज की बातें’ यानी चुभते हुए लाक्षणिक संवाद (विट्स) तथा हास-परिहासपरक गद्य रचनाएँ, व्यंग्य और चुटकिले प्रकाशित कराए जिन्हें सन् 1875 से 1880 के बीच उन्होंने ‘परिहासिनी’ नामक पुस्तिका में संग्रहीत किया।
‘परिहासिनी’ के मुखपृष्ठ पर उन्होंने ‘विनोदार्थ हास-परिहास, चोज की बातें और चुटकिले’ लिखकर चालाक खेल खेला। उक्त पुस्तक में ‘अंगहीन धनी’ और ‘अद्भुत संवाद’ जैसे भी कुछ ऐसे भी मीठे पान थे, जिनमें गुलकंद के रूप में वाजीकारक तत्व था, उत्प्रेरक और उद्वेलक। भारतेंदु द्वारा अपने समय के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं का पुस्तक रूप में उपलब्ध होना कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ उस संकलन से उद्धृत है, ‘अंगहीन धनी’ शीर्षक यह रचना, जोकि अपने समय के सरोकारों से युक्त है—
एक धनिक के घर उसके बहुत-से प्रतिष्ठित मित्र बैठे थे। नौकर बुलाने को घंटी बजी। मोहना भीतर दौड़ा, पर हँसता हुआ लौटा।
और नौकरों ने पूछा, “क्यों बे, हँसता क्यों है?”
तो उसने जवाब दिया, “भाई, सोलह हट्टे-कट्टे जवान थे। उन सभों से एक बत्ती न बुझे। जब हम गए, तब बुझे।”
लेखन और संपादन का ‘परिहासिनी’ जैसा कौशल भारतेंदु के बाद अन्य अनेक लेखक, संपादक उपयोग में लाते और अंग्रेज परस्तों की आँख में धूल झोंकने की चेष्टा करते रहे। इसका एक प्रमाण राकेश पाण्डे ने अपनी पुस्तक ‘ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित साहित्य में गाँधी’ में किया है। उन्होंने सन् 1941 में प्रतिबन्धित एक ऐसी पुस्तक से कुछ सामग्री प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत की है, जिसके आवरण पर उसका नाम ‘वैद्य की लाचारी’ छपा है जबकि भीतरी पन्नों पर ‘बिरहा’ शैली में क्रांतिकारी गीत आदि छपे हैं।
हिन्दी समाज को भारतेंदु ने अलग ही ढंग से चेताने और समकालीन लेखकों को भी स्वयं सरीखा संस्कार देने का प्रयास किया था; लेकिन उनके बाद 1947-48 ई. में हरिशंकर परसाई के आने तक वह सरस्वती लगभग लुप्त ही रही।
समय के साथ-साथ गद्य के उद्देश्यों में भी परिस्थितियों के अनुसार बदलाव नजर आते हैं। भारतेन्दु ने अपने समय में प्रचलित अनेक ‘चुटकुलों’ के साथ मिलाकर कुछ उद्देश्यपूर्ण ‘चुटकिले’ भी लिखे। ‘परिहासिनी’ में प्रचलित चुटकुलों के साथ अनेक स्वरचित उद्बोधक चुटकिलों को सम्मिलित करने का उनका उद्देश्य उस समय के उन राजभक्तों की आँख में धूल झोंकना रहा होगा जो अपने अंग्रेज आकाओं की नजर में खरा बने रहने की कवायद में कवियों-लेखकों-पत्रकारों और प्रेस पर निषेधाज्ञा लागू करने-कराने के नये-नये बहाने तलाशते थे। खेद है कि भारतेंदु की यह ‘चुटकिला मुहिम’ उनसे आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने जहाँ पराधीन भारत को जगाने की दिशा में कुछ सोद्देश्य चुटकियाँ लिखी थीं, वहीं उनके परवर्ती प्रेमघन जी जैसे कथाकारों ने उन्हें मात्र मनोरंजनार्थ माना, समझा और मनोरंजनार्थ ही लिखा। आगे, निरर्थक मनोरंजन से क्षुब्ध पं॰ प्रतापनारायण मिश्र ने अपने पत्र ‘ब्राह्मण’ के एक अंक में लिखा—‘जी बहलाने के लेख हमारे पाठकों ने बहुत-से पढ़ लिये। यद्यपि इनमें भी बहुत-सी समयोपयोगी शिक्षा रहती है, पर वाग्जाल में फँसी हुई ढूढ़ निकालने-योग्य। अत: अब हमारा विचार है कि कभी-कभी ऐसी बातें भी लिखा करें जो इस काल के लिए प्रयोजनीय हैं तथा हास्यपूर्ण न होके सीधी-सादी भाषा में हों।’
(आगामी अंक में जारी…)